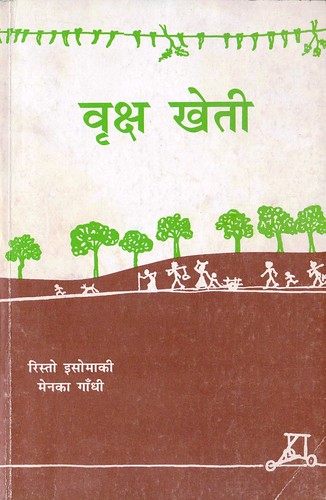सावधान पंजाब सुलग रहा हैा
 |
| पीपुल्स समाचार 28 जुलाई 15 |
 |
| Ptrabhat , Meerut, 2-8-15 |
बीच में रावी नदी है। इस तरफ है गुरदासपुर का गुरूद्वारा डेरा बाबा नानक और नदी के दूसरे तट पर है पाकिस्तान के नारोवाल जिले का गुरूद्वारा करतारपुर। यहां बाबा नानक के अंतिम सांस ली थी। भले ही ये दो अलग मुल्क दिखते हैं, लेकिन रावी पार कर इधर से उधर जाना कोई कठिन नहीं है। देानों देष के सिख सुबह-सुबह अपने गुरूद्वारे से दूसरे को सीस नवांते हैं। यहीं सक्रिय है चार संगठन - खलिस्तान जिंदाबाद फोर्स (रणजीत ंिसह), खलिस्तान टाईगर फोर्स(जगतार सिंह तारा), बब्बर खालसा इंटरनेशनल(वधवा सिंह) और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स(हरमिंदर सिंह मिंटू)। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत द्वारा वांछित सूची के कई आतंकवादी यदि उस पार सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं तो यह उस सरकार की रजामंदी के बगैर हो नहीं सकता। बीते एक दशक के दौरान पंजाब में युवाओं का खेती से मोह भंग हुआ, कनाड़ा व दीगर देशों में जाने का लालच बढ़ा और अचानक ही सीमापार से अफीम व अन्य मादक पदार्थों की आवक बढ़ी। अफगानिस्तान हो या पूर्वी अफ्रीका या फिर पंजाब, हर जगह आतंकवाद हर समय नशाखोरी पर सवार हो कर ही आया है। पंजाब में नशे की तिजारत को ले कर खूब सियासत भी हुई, कई बड़े-बड़े नामों तक इसकी आंच भी गई। गौर करें किसन 1993 में पंजाब से लगी पाकिस्तान की 466 किलोमीटर की सीमा पर कंटीली बाढ़बंदी व फ्लड लाईटें लगाने का काम पूरा हो गया था, और उसके बाद वहां कीाी भी घुसपैठ की कोई शिकायत आई नहीं। बेअंत सिंह की हत्या के बाद राज्य में यही बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, वह भी लगभग 20 साल बाद।
हम यह मान लेते हैं कि गुरदासपुर की घटना का पंजाब में आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मन यह कैसे मान लेगा कि आपरेशन ब्लू स्टार की 31 बरसी के मौके पर अभी दो महीने पहले ही स्वर्णमंदिर में जम कर खालिस्तान के पक्ष में नारे लगे थे और ऐसे 22 युवाओं को केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने चिन्हा भी है। ये सभी युवा बेकार थे व शान की जिंदगी जी रहे हैं। इनके खातों में कनाड़ा व कुछ अन्य देशों से पैसा आता है। ‘‘खालिस्तान. नेट’’ और ‘सर्च सिखिस्म.काॅम’’ जैसे दर्जनभर वेबसाईट, फॅेसबुक पर ऐसे आाधा सैंकडा पेज खुलेआम चुगली करते हैं कि पंजाब में सबकुछ इतना भी सामान्य नहीं है। अब गुरूदासपुर की घटना को ही लें, सुरक्षा बलों ने तीन को मार कर ‘‘जयकारा’’ लगा दिया, लेकिन एक सामान्य बुद्धि इंसान भी भांप जाएगा कि इस पूरी साजिश में कहीं ज्यादा लोग थे।
यदि ये तीन गुरदासपुर के रषश्ट्रीय राजमार्ग पर दो घंटे कोहराम मचा कर थाने में घुस गए थे तो रेल की पटरियों पर बाकायदा बिजली के तारों के साथ डिटोनेटर बांधने का काम कब व किसने किया था। यह भूल जाएं कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, लेकिन यह कटु सत्य है कि आतंकवादी धर्म की घुट्टी पीकर ही अराजक व पिषाच बन जाते हैं। ए वरिश्ठ खुफिया अधिकारी की तात्कालिक टिप्पणी है कि पूरी योजना में सीमा पार करवाने से ले कर जीपीआरएस सिस्टम मुहैया करवाने, रैकी करने आदि में कम से कम 15 लोग का काम है यह और इसमें से कई स्थानीय ही हैं। षायद पाठक भूले नहीं होंगे कि ब्लू स्टार की बरसी के ठीक पहले जम्मू में उस अवसर पर जलसे की तैयारी कई दिनों पहले से की गई। पंजाब में कुछ सालों से किस तरह सरहद पार बैठे लोग खलिस्तान को कब्र से निकाल कर जिलाना चाहते हैं, यह भी दबा-छुपा नहीं है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हो ही गई कि सीमावर्ती जम्मू के रानीगंज व नवांषहर में पांच दिन तक हिंसा चलती रही। एक युवक मारा गया, एक सुरक्षा अधिकारी की एके-47 राईफल छीन ली गई। कष्मीर में अलग राज्य की मांग करने वाले वाले पंजाब में अलग खालिस्तान की मांग व षहीदी समागम के नाम पर भिंडरावाले , षुबेग सिंह सहित कई आतंकवादियों का महिमामंडन करने में हमारी सरकारों का भेदभाव कहीं हालात को और ना बिगाड़ दे।
जरा कुछ महीनों पीछे ही जाएं, सितंबर- 2014 में बब्बर खालसा का सन 2013 तक अध्यक्ष रहा व बीते कई दषकों से पाकिस्तान में अपना घर बनाएं रतनदीप सिंह की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की। उसके बाद जनवंबर- 14 में ही दिल्ली हवाई अड्डे से खलिस्तान लिबरेषन फोर्स के प्रमुख हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू को एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। ये लेाग थाईलैंड से आ रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सजायाफ्ता व सन 2004 में अतिसुरक्षित कहे जाने वाली चंडीगढ की बुढैल जेल से सुरंग बना कर फरार हुए जगतार सिंह तारा को जनवरी-2015 में थाईलैंड से पकड़ा गया। एक साथ विदेषों में रह कर खालिस्तानी आंदोलन को जिंदा रखने वाले षीर्श आतंकवादियों के भारत आने व गिरफ्तार होने पर भले ही सुरक्षा एजेंसिंयां अपनी पीठ ठोक रही हों, हकीकत तो यह है कि यह उन लोगों का भारत में आ कर अपने नेटवर्क विस्तार देने की येाजना का अंग था। भारत में जेल अपराधियों के लिए सुरक्षित अरामगाह व साजिषों के लिए निरापद स्थल रही है। रही बची कसर जनवरी-15 में ही राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाष सिंह बादल ने 13 कुख्यात सजा पाए आतंकवादियों को समय से पहले रिहा करने की मांग कर दी थी जिसमें जगतार सिंह तारा भी एक था। कुल मिला कर देखे तो जहां एक तरफ राज्य सरकार पंथक एजेंडे की ओर लौटती दिख रही है तो इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की जड़ तक जाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं।
अभी तीन दिन पहले ही पटियाला विष्वविद्यालय में मुख्यमंत्री श्री बादल की मौजूदगी में ुकछ लोगों ने अलग खालिस्तान के पक्ष में जम कर नारेबाजी की थी। दीनानगर को अपनी कार्यवाही के लिए चुनने का कारण महज यह नहीं है कि यह सीमा के करीब है। असल में यह कस्बा कभी महाराज रणजीत सिंह की राजधानी रहा है। इसके आसपास गुरू नानकदेव व अन्य सिख गुरूओं से जुड़ी कई यादें हैं व सीमा से सटे पाकिसतान के गांवों में खासी सिख आबादी भी है। यह भी संभव है कि इस घटना में खालिस्तानियों का हाथ ना हो लेकिन इसने उनके लिए उत्प्रेरक का काम तो किया ही है। पंजाब में सत्ताधारी दल जिस तरह से भुल्लर की आवभगत कर रहा है, राज्य से चार सांसद लोने वाले आम आदमी पार्टी के कुछ नेता सरेआम खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते रहे हैं, इससे साफा जाहिर है कि राज्य में कुछ अपराधियों, कुछ विघ्नसंतोशियों व कुछ देषद्रोहियों को एकजुट कर जहर घाोलना कतई कठिन नहीं है। अभी समय है और साधन भी वरना पंजाब जैसे तरक्कीपसंद, जीवट वाले राज्य को फिर से आतंकवादियों का अड्डा बनने से रोका जाना आसान भी है और जरूरी भी।